दर्शन (darshan explained in hindi):
सांसारिक दृष्टिकोण हेतु, नेत्रों की आवश्यकता होती है लेकिन, जो दिखाई दे रहा है उससे, कैसा संबंध रखना है, यह केवल दर्शन के माध्यम से ही समझा जा सकता है| आपने देखा होगा, जो बात आपके लिए अधार्मिक है वह, किसी और के लिए गर्व का अनुभव देने वाली होगी| भला, दो मनुष्यों में इतना भेद कैसे? जबकि, जानवरों की किसी भी प्रजाति के लिए, जो सच है, वह सभी के लिए, एक समान होता है किंतु, मनुष्य के लिए, दुनियाँ विभिन्नता क्यों? तो आपको बता दें, इसका कारण मानवीय दृष्टिकोण है जो, दर्शन शास्त्र के ज्ञान से ही प्राप्त होता है| भारत में द्विपक्षीय दर्शन को महत्व दिया गया जहाँ, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत, पाँच दर्शन और नास्तिकता को प्रमाणित करने वाले, तीन दर्शन उपलब्ध हैं जिन्हें, निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे|
- दर्शन क्या है?
- दर्शन का महत्व क्या है?
- दर्शन कितने होते हैं?
आस्तिक दर्शनः
- सांख्य दर्शन क्या है
- योग दर्शन क्या है
- न्याय दर्शन क्या है
- वैशेषिक दर्शन क्या है
- मीमांसा दर्शन क्या है
- वेदान्त दर्शन क्या है
नास्तिक दर्शनः
- चावार्क दर्शन क्या है
- बौद्ध दर्शन क्या है
- जैन दर्शन क्या है

संसार में चारों ओर मनुष्य दुखी है| वह सम्पूर्ण जीवन सुख की तलाश में, सुनी सुनाई बातों पर आगे बढ़ता रहता है और फिर, जब सांसारिक भोग से मन तृप्त नहीं होता तो, अपने जीवन में किए गए कर्मों पर, पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता| मनुष्य के दुख का कारण, दर्शनों में भेद न करने की वजह से है| जब किसी वस्तु की फोटोग्राफी करना हो तो, उसे चारों दिशाओं से देखा जा सकता है किंतु, सभी दिशाओं में कैमरे का एंगल बदलना होगा तभी, फ़ोटो खींची जा सकेगी| उसी प्रकार अपने ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग है किंतु, सभी की प्रक्रिया समझना अनिवार्य है| वस्तुतः एक ही भांति की सोच, सभी मनुष्यों के लिए, उचित नहीं होती| दर्शन ही एक ऐसा मार्ग है जो, मनुष्य को पशुओं से विभिन्न बनाता है अन्यथा शारीरिक तल पर तो, इंसानों और जीव जन्तुओं में कोई भेद नहीं| मनुष्य के विचार ही उसे श्रेष्टता प्रदान करते हैं और विचारों की उत्पत्ति, प्राचीन ऋषियों और दार्शनिकों द्वारा दिए गए अभिलेखों से ही होती है| जिसका जाने अनजाने में, सभी मनुष्य पालन करते हैं| अतः दर्शन का पूर्ण ज्ञान होने से, दुनिया को सही मायने में पहचाना जा सकता है| निम्नलिखित बिंदुओं में इस तथ्य का स्पष्टीकरण उपलब्ध है|
दर्शन क्या है?

मानवीय दृष्टिकोण ही, दर्शन कहलाता है| संसार को कोई व्यक्ति किस भाव से देखेगा, यह केवल दर्शन से ही तय किया जाता है| जैसे मोबाइल का उपयोग, सामान्य व्यक्ति मनोरंजन के लिए करेगा किंतु, शेयर मार्केट या सोशल मीडिया विशेषज्ञ है तो, वह उस मोबाइल से धन अर्जित करने का मार्ग तैयार कर लेगा| यह केवल मानव दृष्टिकोण है जो, किसी भी विषय वस्तु को, अपने पूर्वनियोजित ज्ञान के आधार पर ही, सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकता है| संसार में सभी तत्वों से, उचित सम्बन्ध बनाना आवश्यक होता है अन्यथा जीवन दुखों के सागर में, तैरते ही बीत जाता है| जैसे, कोई लड़का जवानी की आयु में, किसी लड़की की ओर देखता है तो, आकर्षित होता है किंतु, यदि वह खेल या शिक्षा में केंद्रित हो तो, उसका ध्यान कहीं नहीं जाएगा| किसी वस्तु को खाना है या स्पर्श करना या केवल दूर से देखना मात्र है, इन सभी बातों का बोध होना अति आवश्यक है क्योंकि, मनुष्य अपने अभिमान में केवल, अपने आस पास के लोगों से ग्रहण किए हुए ज्ञान को ही, प्रमुखता देता है जबकि, मनुष्य ने सहस्र वर्षों पूर्व ही ज्ञान देना सीखा है और पृथ्वी करोड़ों वर्षों से यूँ ही चल रही है जिसमें, बहुत बड़ा योगदान ज्ञानी मनुष्यों का भी रहा है, जिनके बलिदान ने, मानव समाज को अपनी चेतना को पहचानने योग्य, नेत्र दिए अन्यथा मनुष्य तो, लाखों वर्षों से, जानवरों की भांति जीता चला आ रहा था किंतु, जैसे ही, कृषि संपन्नता बढ़ी तो, मानव मन तृप्ति की माँग करने लगा और तभी से, दर्शन का प्राम्भ हुआ| महान ऋषियों ने जिन मार्गों पर चल कर, आनंद का अनुभव किया, वही मार्ग राम, कृष्ण, बौद्ध, महावीर इत्यादि के द्वारा बताया गया लेकिन, किसी एक का कठोरता से पालन न करने से ही, व्यक्ति संसार को सही मायने में देख नहीं पा रहा| विभिन्न रंगों के चश्मे पहनने से, संसार का रंग भेद ज्ञात नहीं किया जा सकता| अतः सभी चश्मों को उतारकर केवल, एक ज्ञान का चश्मा धारण करना ही श्रेष्ठ दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसे, दर्शन के रूप में व्यक्त किया गया है|
दर्शन का महत्व क्या है?

जैसा कि, उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि, दर्शन ही मानवीय दृष्टिकोण होता है और बिना दृष्टिकोण के, संसार पहचाना नहीं जा सकता और संसार को जाने बिना, आनंदित होकर जीना तो असंभव है हालाँकि, प्रारंभिक तौर पर कुछ सूचनायें आस पास के वातावरण या स्वाध्याय से भी प्राप्त हो जाती है| संसारी इसी सीमित ज्ञान की सहायता से, अपना जीवन सुख दुख में रहते हुए ही काट देते हैं| उन्हें लगता है कि, कदाचित् यह उनके पिछले जन्मों का कर्म होगा या उनसे, कोई त्रुटि हुई है जिससे, वह जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित रह गए जबकि, यह व्यक्ति की निजी कल्पना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं| यदि जीवन को सही मायने में जानना है तो, दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है| कई दिव्य आत्माओं ने, अपने सम्पूर्ण जीवन के त्याग से, ऐसे आनंदमयी मार्ग खोजें जो, मनुष्य को उसके कष्टों से मुक्ति दे सकते हैं किंतु, जब तक दुनिया को, उसके वास्तविक रूप में न देखा गया तो, भ्रम होना संभव है जो, आगे चलकर मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बनता है इसलिए, दर्शनशास्त्र के शिक्षा, प्रत्येक मनुष्य के लिए, अति आवश्यक हो जाती है जिसे, इस लेख में संक्षिप में वर्णित किया गया है|
दर्शन कितने होते हैं?
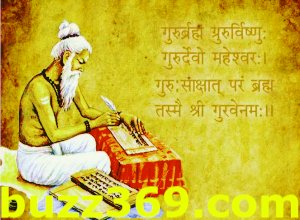
संसार में रहने के कई मार्ग हैं| जैसे- वैराग्य, दाम्पत्य या विक्षिप्त जहाँ, अधिकतर मनुष्य मिश्रित विचारधाराओं के साथ, विक्षिप्त स्थिति में विचरण करते हैं लेकिन, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिन्होंने, केवल एक विचारधारा का पालन करके, अपने जीवन को श्रेष्टतम आनंद तक अवश्य पहुंचाया होगा| सामान्य मनुष्य, लोगों को देखकर उनकी निंदा करते हैं किंतु, वह भूल जाते हैं कि, संसार में उपस्थित सभी गुण, परमात्मा की शक्ति से ही संचालित होते हैं, तो भला उनमें भेद क्यों करना? जैसे, किसी को पढ़ने में रस प्राप्त होता है तो, किसी को मनोरंजन में और तो और कोई ऐसा भी होगा जो, अपने जीवन से हताश होकर, मुक्ति की माँग कर रहा होगा लेकिन, कोई भी व्यक्ति आत्मावलोकन के आभाव में, किसी भी मार्ग को अपनाता है तो, वह निश्चित ही, कुछ दिनों के बाद अपने ही कर्मों से निराश हो जाएगा| फिर वह झूठे प्रोत्साहन देने वाले, विषयों का उपयोग करेगा जो, उसकी अधोगति का कारण बनेंगे| अतः अहंकार और मोह की निद्रा त्याग कर ही, अपनी यथास्थिति देखने का प्रयत्न करना चाहिए किंतु, कैसे? क्योंकि, आप अपने आपको वही समझते हैं जो, लोगों ने आपको बताया है| तो भला इसके अतिरिक्त, कुछ और कैसे सोचा जा सकता है? तो, आपको बता दें कि, यहीं से दर्शनों का आरंभ होता है जो, मनुष्य के जीवन को एक सार्थक बिंदु की ओर निर्देशित कर सकते हैं| दर्शनों का वर्गीकरण, उनकी उपयोगिता के आधार पर किया गया है| संसार को चलने के लिए, सभी सांसारिक तत्वों का परस्पर अनुकूल संबंध होना अनिवार्य है अन्यथा पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र, अस्थिर हो जायगा जैसा कि, आप जानते होंगे, पृथ्वी का जलस्तर 72 प्रतिशत है और यदि मानवीय शरीर का जल स्तर देखा जाए तो, वह भी पृथ्वी के अनुपात में बराबर ही प्रतीत होता है| यह एक बात का संकेत है कि, मानव शरीर ही पृथ्वी का प्रतिबिम्ब है| जिस प्रकार पृथ्वी को सुचारु रूप से चलने के लिए, सभी तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी, आनंदित रहने के लिए, संपूर्ण सृष्टि की आवश्यकता होगी| लेकिन, जब मनुष्य केवल कुछ लोगों में ही, अपना जीवन तलाशने लगता है तो, वह माया के भ्रम में घिर जाता है| जहाँ से, उसके दुखों की उत्पत्ति होती है इसलिए, विभिन्न दार्शनिकों के जीवन को, सांसारिक मार्गदर्शन माना गया जहाँ, इसे दो रुप में विभाजित किया गया है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन जिन्हें, कई विचारधाराओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है| आइए इसे जानते हैं|
आस्तिक दर्शन:

आस्तिक अर्थात ईश्वर पर आस्था रखने वाला मनुष्य, इसके अंतर्गत छः दर्शनों का समावेश है जिन्हें, षड्दर्शन भी कहा जाता है| ईश्वर पर आस्था रखना तो, एक श्रेष्ठ कर्म है किंतु, जब आस्था अन्धविश्वास बनने लगे तो, वह विनाशकारी सिद्ध होती है इसलिए, ऊपर वाले को समझने के लिए, सभी दर्शनों का ज्ञान होना अनिवार्य है अन्यथा दूसरी विचारधाराओं के लोगों को, हीन मानने से विवादित स्थिति बने रहना संभव है| संसार में कोई भक्ति का मार्ग अपनाता है तो, कोई भोग का, दोनों ही मार्ग मनुष्य को, उच्चतम आनंद प्रदान कर सकते हैं लेकिन, जब तक उनका सत्यता से ज्ञान न हो तो, वह उसी प्रकार होंगे जैसे, बंदर के हाथ में मोबाइल| आइए हम एक एक करके, सभी विचारधाराओं को जानने का प्रयत्न करते हैं|
सांख्य दर्शन क्या है?

ईश्वर को द्वैत या अद्वैतवादी मार्ग से जाना जा सकता जहाँ, सांख्ययोग द्वैतवादी विचारधारा का समर्थन करता है| जिसके अंतर्गत संसार को विभिन्न रूपों में देखना ही, सांख्य दर्शन कहलाता है| यहाँ ईश्वर को, बाहर खोजा जाता है सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का वर्णन मिलता है| पुरुष वह जो, संसार को देखता है और प्रकृति वह जिसे, पुरुष देख रहा है| यहाँ कई पुरुष हैं, जिनकी समुचित गणना को, संख्याओं से प्रदर्शित किया गया है| सांख्य दर्शन में, वैज्ञानिक तर्कों का समावेश मिलता है जहाँ, गुणों की उत्पत्ति गुण से ही मानी गई है| एक ही प्रकृति की, विकृति से, संस्कृति का निर्माण होता है| जिस प्रकार एक पेड़ को काटने से, कई आकृतियां बनायी जा सकती है और उनके गुणों में भेद भी व्यक्त किया जा सकता है| उसी प्रकार ईश्वर की माया, विभिन्न रूपों में प्रतीत होती है, जितने मनुष्य, उतने पुरुष| यहाँ पुरुष का अर्थ लिंगातमक नहीं बल्कि, दृष्टा से लिया गया है जो, संसार को देखने वाला है, वही पुरुष है| एक व्यक्ति के लिए, कोई दूसरा व्यक्ति, वस्तु या स्थान प्रकृति ही होगा और इनसे उचित संबंध ही, जीवन को आनंद प्रदान कर सकता है जिसे, मुक्ति कहा गया है चूँकि, बंधन तो किसी भी जीव की, कष्टकारी स्थिति का सूचक होता है और संसार में उपस्थित मनुष्य, अपनी मुक्ति के लिए ही, सांसारिक विषयवस्तुओं से संबंध स्थापित करता है किंतु, सांख्य दर्शन का अध्ययन किए बिना, प्रकृति से मधुर सम्बन्ध बनाना असंभव है| सांख्य दृष्टिकोण, प्रकृति को सत्य की श्रेणी में रखता है जहाँ, संसार को नित्य कहा गया है जो, सदा से हैं और हमेशा रहेगा| जो, एक अर्थ में बिलकुल उचित है क्योंकि, पुरुष के लिए तो संसार हमेशा होता है| भला कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि, यह संसार मिथ्या है, नहीं न? यह संसार केवल अद्वैतवादी मनुष्य के लिए ही, मिथ्या हो सकता है लेकिन, सांसारिक मनुष्यों को, दुनिया को झूठा कहने का कोई अधिकार नहीं| जिसे अब भी दुनिया में भेद दिखाई दे रहा हो, उसके लिए संसार में घटने वाली घटनाएँ भी, वास्तविक होंगी और उनका प्रभाव भी, उसके जीवन पर निश्चित ही पड़ेगा| जैसे, सांसारिक मनुष्य अपने अपने संप्रदायों के अनुसार, एक निश्चित समय में शिक्षा और विवाह जैसे, निर्णय लेते हैं| यह मानव व्यवस्था के लिए, आवश्यक है किंतु, यदि कोई अपने आपको लड़का या लड़की न मानकर, किसी कर्म में समर्पित हो तो, उसे अपने निजी जीवन से कोई सरोकार नहीं होगा| यहाँ अंतर केवल विचारधारा का है, जिसकी उत्पत्ति दर्शन से ही होती है| सांख्य दर्शन को मानने वाले मनुष्य के लिए, समय का सर्वाधिक महत्व होता है क्योंकि, वह अपनी आयु के विभिन्न पड़ावों पर, स्थितियों को पूर्वावलोकन करके बैठे होते है जिसके पूरा होने के लिए, समय का ध्यान रखना अनिवार्य हो जाता है| पुरूष प्रकृति के बदलाव को देखता है जिसे, समय के रूप में व्यक्त किया गया है| अतः संसार में रहने वाले व्यक्तियों को, धर्म के अंतर्गत कर्म करने होंगे जिससे, जीवन सुचारु रूप से आगे बढ़ सके, यही सांख्य दर्शन का सार है|
योग दर्शन क्या है?

योग अर्थात जुड़ाव जहाँ, परमात्मा से आत्मा का मिलन हो, वही योग है| योग दर्शन एक ऐसा ज्ञान है, जिसके माध्यम से, सांसारिक विषय वस्तुओं को, उनके यथार्थ रूप में अपनाया जा सकता है| सांख्य बोध से अतृप्त मन, योग दर्शन की ही शरण लेता है ताकि, वह जीवन के मिथ्यात्व को भलीभाँति देख सके और दुख के बंधनों से बाहर आ सके| जिस प्रकार हनुमान, श्रीराम के और अर्जुन, श्रीकृष्ण के योग से, सांसारिक दुखों से मुक्त हुए, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को, अपने जीवन में किसी सत्य कर्मी व्यक्ति या नित्य उद्देश्य से, घनिष्ठ संबंध स्थापित करने ही होंगे तभी, योग घटित होगा| योग, किसी प्रकार का ज्ञान ग्रहण करना नहीं बल्कि, अपना समर्पण करना है जिससे, मनुष्य का अहंकार निष्क्रिय हो सके चूँकि, प्रकृति का ज्ञान तो, सांख्ययोग से भलीभाँति प्राप्त किया जा सकता है| अतः योग सांसारिक बंधनों से, विखंडन का मार्ग है| मनुष्य सत्त्व, रज, तम तीनों गुणों के प्रभाव से ही, संसार से संबंध स्थापित करता है लेकिन, जब मनुष्य अनंत विषयों से लिप्त हो करके भी, तृप्त नहीं होता तो, उसे अपने जीवन से घृणा होने लगती है और वह अपने मन को, शांत करने के लिए, अपने जीवन से मुक्ति की माँग करने लगता है जो, मनुष्य की वास्तविकता है| जिसका संबंध, मानवीय गुणों से न होकर, मनुष्य के स्वभाव से होता है| योग दर्शन मनुष्य का मृत्यु भय समाप्त कर, उसे अनंतता की ओर प्रशस्त करता है जहाँ, मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से बाहर आकर, किसी सत्य आधारित कर्म की सक्रियता में ही, अपने जीवन की सार्थकता तलाशता है| यही योग दर्शन है|
न्याय दर्शन क्या है?

संसार में ईश्वर प्राप्ति के मार्गों में, एक न्याय दर्शन भी कहलाता है जहाँ, ईश्वर पर विश्वास करने के लिए, कुछ मानको का निर्धारण किया गया है, जिनके अनुसार ही, ईश्वर के बारे में जाना जा सकता है| न्याय दर्शन प्रत्यक्षता पर दबाव देता है जहाँ, यथार्थ रूप में देखी गई आकृति पर ही, विश्वास किया जाता है किंतु, पाया गया कि, दृश्य भ्रमित भी कर सकता है इसलिए, दृश्य से संबंधित कई अनुमानों को भी, जाँचा जाता है जहाँ, किसी और विषय से तुलना कर, विशेषज्ञों के शब्द प्रमाण के माध्यम से, सत्य तक पहुँचने का प्रयास होता है| यही न्याय दर्शन का सिद्धांत है| न्याय दर्शन, तर्क शक्ति और बुद्धि बल पर आधारित ज्ञान प्राप्त करने को, प्राथमिकता देता है| न्याय दर्शन की रचना, ऋषि अक्षपाद एवं गौतम जी द्वारा की गई थी जो, आज संपूर्ण मानव जाति को विज्ञान से अवगत कराती है|
वैशेषिक दर्शन क्या है?

न्याय दर्शन की आपूर्ति ही, वैशेषिक दर्शन को जन्म देती है जहाँ, न्याय दर्शन प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित विषय वस्तुओं को ही, सत्य समझता है वहीं, वैशेषिक दर्शन विशेष पदार्थ की बात कहता है जिसे, विज्ञान की दृष्टि से देखा नहीं जा सकता और न ही, विज्ञान उसकी कल्पना कर सकता जो, आकाश की अनंतता या अंतरिक्ष के विस्तार के रूप में भी, जाना जा सकता है| विज्ञान के तर्क के अनुसार, संसार का कोई भी तत्व, दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर ही बनता है लेकिन, जो अणु का अंतिम भाग है जिसका, कोई विखंडन न किया जा सके अर्थात जिससे, संसार की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में न्याय दर्शन मौन रह जाता है| उसी श्रेष्ठतम तत्व के अध्ययन को, वैशेषिक दर्शन में स्पष्ट किया गया है|
मीमांसा दर्शन क्या है?

मीमांसा के अंतर्गत, वेदों का पुनर्जागरण सम्मिलित है जहाँ, धार्मिक कर्मकांडों का विशेष महत्व बताया गया हैं| जब संसार में नास्तिकतावादी विचारधाराएँ पनपने लगीं तभी, मीमांसा की उत्पत्ति हुई जहाँ, वेदों की श्रेष्टता को उजागर किया गया और मानव समाज को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए, प्रेरित किया गया ताकि, वेद ज्ञान, विलुप्त होने से बचाया जा सके| मीमांसा में कई तरह के यज्ञों और पूजा विधियों का वर्णन मिलता है जिसे, भगवत प्राप्ति का मार्ग कहा गया है| मीमांसा दर्शन में, कर्मों पर आधारित जीवन श्रेष्ठ माना गया है| जैसे, किसान का खेती करना, एक वैज्ञानिक का आविष्कार करना, सैनिक का रक्षा करना इत्यादि| मानव अनुकूल वातावरण के लिए, ज्ञान के साथ साथ पोषण और सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है जो, एक दूसरे के परस्पर समन्वय से ही, प्राप्त की जा सकती है| मीमांसा, पारिवारिक संबंधों को भी अनिवार्यता प्रदान करता है जहाँ, अपने पूर्वजों की सेवा से लेकर, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने हेतु प्रेरित करना ही, धर्म माना गया|
वेदांत दर्शन क्या है?

वेदांत दुनिया का अंतिम सत्य है जिसे, आत्मा या सनातन से भी संबोधित किया जा सकता है| वेदांत दर्शन का प्रारंभ जिज्ञासा से होता है जहाँ, सांख्य को मानने वाले लोग, अपने द्वारा बनाए गए धार्मिक केन्द्रों को ही, चेतना स्थल मानते हुए, साकार रूप में ईश्वर की कल्पना करते हैं वहीं, वेदांत मार्गी सभी मान्यताओं पर, प्रश्नचिन्ह लगाकर आगे बढ़ते हैं जिससे, वह संसार के माया जाल को देख पाते हैं| वेदांत न संस्कृति है, न ही कोई परंपरा, न तो काल और न ही कोई भौतिक काया, वेदान्त तो वह तत्व है जिसे, अनंतता से ही प्राप्त किया जा सकता है जो, व्यक्तिगत अहंकार के निष्क्रिय होते ही, उद्दीप्त होगा हालाँकि, जो कभी खोया ही नहीं, उसे प्राप्त करने वाला कथन अतार्किक है किंतु, वेदांत उस कस्तूरी की भांति है जो, मृग के पास होते हुए भी, चारों ओर उसकी तलाश करता है| धार्मिक दृष्टिकोण से, वेदांत दर्शन ब्रह्म प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है जहाँ, भक्त वेदों के गहन अध्ययन से, संसार की व्यर्थता से अवगत होते हैं और अद्वैतवादी विचारधारा का पालन करते हुए, अपने कर्म सिद्धांत का चुनाव करते हैं| वेदांत दर्शन संसार को मिथ्या मानता है अर्थात संसार, जैसा दिखाई देता है, वैसा होता नहीं| मिथ्या और असत्य में यही अंतर है जहाँ, असत्य को सत्य से निष्कासित किया जा सकता है लेकिन, मिथ्या को नहीं क्योंकि, अद्वैतवादी के लिए, भले ही संसार असत्य है जिससे, उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता लेकिन, जब तक वह संसार के चक्रव्यूह में फँसा है, जीवन के बंधनों से घिरा है, तब तक उसके लिए, यही संसार वास्तविक होगा और इससे बाहर आने तक, उसे असत्य कहना तर्कसंगत नहीं हो सकता अतः मिथ्या ही कहा जायेगा| वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गुरु का मार्गदर्शन होना अनिवार्य है अन्यथा विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव, अर्थ का अनर्थ करेगा| वेदांत, पुरुष और प्रकृति का ऐसा समन्वय है जिससे, मानव मुक्ति संभव हो सके| वेदांत मार्गी संसार को माया के रूप में देखते हैं जहाँ, उन्हें किसी भी विषय वस्तु में, भेद प्रतीत नहीं होता| उनकी दृष्टि में, सभी एक समान होते हैं| चाहे फिर, वह अतिसूक्ष्म कीट हो या विशालकाय जानवर, सभी के प्रति एक दृष्टि रखना ही, वेदांत दर्शन का मूलाधार है|
नास्तिक दर्शन:

ईश्वर पर आस्था न रखने वाले मनुष्यों को, नास्तिक कहा गया है और इसी विचारधारा का समर्थन करने वाले व्यक्तियों द्वारा, नास्तिक दर्शनों की रचनाएँ की गई| जो आज सम्पूर्ण विश्व में, विस्तारपूर्वक अपनायी जा रही हैं| जब ईश्वर पर आस्था रखने वाले मनुष्य, वैदिक ज्ञान के अभाव में, अंधविश्वास को बढ़ावा देने लगे तो, नास्तिक विचारधारा उत्पन्न हुई जहाँ, कुछ बुद्धिजीवी या विचाराधीन मनुष्यों ने, विज्ञान की शोध करके, पाखंड को पहचान लिया और यही परीक्षण, कभी कभी आस्था पर सवाल उठाने पर विवश करने लगा| वस्तुतः ईश्वर पर विश्वास रखना तो, ज्ञान का मार्ग है जिसे, निश्चल भक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है लेकिन, सांसारिक आडंबर, ईश्वर से कोसों दूर है| जिन स्थानों से मन की शांति प्राप्त होनी चाहिए, वही आज केवल, मनोरंजन का केंद्र बन के रह गए हैं| यह उस परमात्मा का निरादर है, जिसके विरोध में, नास्तिक दर्शनों ने अपनी जगह बनाई हालाँकि, सभी दर्शन अपने दृष्टिकोण से, मनुष्य को परमात्मा तक अवश्य पहुँचा सकते हैं लेकिन, जब कई विचारधाराओं का मिश्रण हो तो भला, एक दृष्टि से संसार कैसे दिखाई देगा| निम्नलिखित बिंदुओं में इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध है|
चार्वाक दर्शन क्या है?

सांसारिक मनुष्यों की भोगवादी विचारधारा से उत्पन्न दृष्टिकोण, चार्वाक दर्शन कहलाते है| जिनमें दिए गए निर्देशों के अनुसार, मनुष्य को आजीवन भोग करना चाहिए हालाँकि, चार्वाक किसी मनुष्य का नाम नहीं, यह ऐसे लोगों का समूह है जो, केवल इस जीवन को मनोरंजन का माध्यम समझते हैं| आपने, अपने आस पास कई लोगों को ऐसी बातें कहते सुना होगा कि, “यार एक दिन मर जाना है, खुलकर अय्याशी करो, यहाँ कोई नहीं हमें देखने वाला” यही सोच चार्वाक दर्शन का सूचक है जहाँ, मुख्य रूप से एक व्याख्यान भी प्रचलित है:- पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, यावत्पतति भूतले।उत्थाय च पुनः पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते॥
जिसका हिंदी अनुवाद है, “जब तक जियो, सुख से जियो, गिरने तक पियो और उठो पुनः पियो क्योंकि, मनुष्य का कोई पुनर्जन्म नहीं तो, इस जन्म को सुख में बिताओ, फिर चाहे उसके लिए, ऋण ही क्यों न लेना पड़े” हालाँकि, यह सब सुनने में तो मनमोहक प्रतीत होता है किंतु, वास्तव में सभी लोग यदि इस दर्शन का पालन करने लगें तो, क्या मानव समाज चल सकेगा? आज हम जो मोबाइल चला रहे हैं वह भी, किसी मनुष्य ने रात दिन परिश्रम करके निर्मित किया होगा| जिस वाहन में यात्राएं कर रहे हैं, वह किसी के संघर्ष का ही परिणाम है और यदि, वह भी इसी विचारधारा के अनुसार, केवल मनोरंजन में ही समय व्यतीत करते तो, इनका निर्माण कैसे होता है और आज हम सभी, पत्थर से टकरा टकरा कर आग जला रहे होते इसलिए, चार्वाक नीति कुछ लोगों के लिए क्षणिक लाभदायी हो सकती है किंतु, जब इसे संपूर्ण मानव जाति अपनाए तो, निश्चित ही इसके विनाशकारी परिणाम होंगे| चार्वाक को, यदि दूसरे पक्ष से देखा जाए तो, यह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो सकता है चूँकि, सांसारिक सुखों में मन की तृप्ति नहीं मिल सकती| यह बात तो, अकाट्य सत्य है इसलिए, जब कोई चार्वाक सोच के साथ, संसार में उतरता है तो, वह बहुत जल्दी अपने जीवन से निराश हो जाता है और दुनिया के सारे सुख सुविधाएँ देखने के बाद भी, जब वह संतुष्ट नहीं होता तो, उसकी अन्वेषक मनोकामना सही दिशा में बढ़ सकती है परिणामस्वरूप उसकी अपूर्ण चेतना, सत्य के प्रति जिज्ञासा प्रकट करती है तभी, एक नए आयाम का आरम्भ होता है और वह जीवन की वास्तविकता को समझ पाता है|
बौद्ध दर्शन क्या है?

गौतम बुद्ध के द्वारा प्रदत्त सिद्धांत, बौद्ध दर्शन कहलाते हैं| महात्मा बुद्ध ने, आठ प्रकार की मार्ग बताए हैं जिनका पालन करने से, मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो सकता है| सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। यहाँ सम्यक् का अर्थ, उचित या न्यायोचित से लिया गया है महात्मा बुद्ध, धार्मिक परम्पराओं के सबसे बड़े निंदक रहे हैं| उनके अनुसार, पूजा विधियों का पालन करना, अतार्किक है| बुद्ध का वैदिक कर्मकांडों पर विशेष आक्षेप था कि, जब भगवान दुखियों का दुख दूर नहीं कर सकता तो, उसकी पूजा क्यों की जाए? हालाँकि, इस कथन से वेदों की गरिमा को क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती| वेदों में कई ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर दे पाना असंभव है अतः केवल उस पर विचार करने से या लिखी हुई बातें मान लेने से, न तो मनुष्य का दुःख कम होगा और न ही, उसे भगवत प्राप्ति होगी| बौद्ध दर्शन नैतिकतावादी विचारधारा का समर्थक है जिनमें, चार आर्य सत्यों की बात कही गई है जिसे, निम्न श्लोक से समझा जा सकता है|
दुक्खं अरियसच्चं, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं, दुक्खनिरोधं अरियसच्चं, तथा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं।
अर्थात जो व्यक्ति चार सत्यों को देखता है| दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुगमन, वही मनुष्य, इस संसार में एक श्रेष्ठ और ऊँचा जीवन व्यतीत कर सकता है| बुद्ध ने जीवन शून्यता को अधिक महत्व दिया है जिनके अनुसार, मनुष्य की कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं होती| एक दिन सभी का शरीर बूढ़ा होकर, कष्ट प्राप्त करेगा इसलिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर, सत्य कर्मों को प्राथमिकता देना ही, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए ताकि, मनुष्य एक दूसरे के लिए, उपयोगी सिद्ध हो सके और सभी का जीवन सुगम बनाया जा सके|
जैन दर्शन क्या है?

जैन दर्शन प्राचीनतम ज्ञान है जिसे, सनातन का ही अंग बताया जाता है| प्रथम जैन तीर्थंकर, ऋषभदेव जिन्होने, जैन दर्शन का उदय किया| जैन दर्शनों में २४ तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है जहाँ, अंतिम तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर हुए| जिन्हें २३वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ का उत्तराधिकारी बनाया गया| जैन दर्शन नास्तिकता का प्रबल समर्थक रहा है| जैन सम्प्रदाय मानवीय कर्मों को प्रमुख मानता है| उनके अनुसार सत्य एक विशालकाय हाथी की भांति है और उसे मानने वाले, अंधे मनुष्य के रूप में, चित्रित किये गये हैं| चित्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया कि, सत्य किसी एक के समझे जाने योग्य नहीं हैं बल्कि, जो जिस रुप में उसे देखता है उसके लिए, वही सत्य है| कोई अंधा हाथी की पूँछ पकड़कर कहेगा कि, हाथी तो पतली सी रस्सी की भांति है, जिसने हाथी के पैर पकड़े होंगे, वह कहेगा हाथी तो, एक खंभा है और जिसने, हाथी के दाँतों को स्पर्श किया होगा, वह कहेगा कि, हाथी कोई नुकीली लकड़ी है अर्थात सभी मनुष्यों ने, सत्य के कुछ अंश को ही जाना है चूँकि, सत्य अनंत है जिसका संपूर्ण अध्ययन संभव नहीं अतः सत्य ढूंढने से उत्तम है कि, सद्भावना से अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि, जीवन को आनंदित रखा जा सके| जैन दर्शन के तीन प्रमुख अंग बताए गए हैं, ज्ञानमीमांसा, तत्वमीमांसा और नितिमीमांसा, जिनका संयुक्त अध्ययन, मुक्ति या मोक्ष की ओर, अग्रसर होने में सहायक है| जैन दर्शन के अनुसार, सत्य को दो तरह की कसौटी से, जाँचा जाएगा| पहला, उसका जन्म और मृत्यु से संबंध होना चाहिए| दूसरा, उसके अंदर कुछ ऐसा हो जो, न कभी जन्मा हो और न कभी समाप्त किया जा सके अर्थात जो नित्य है, उसे ही सत्य कहा जा सकता है इसलिए, एक जैन संप्रदाय मनुष्य के रूप में ही, भगवान को देखते हैं जिन्हें ,तीर्थंकर माना जाता है|
उपरोक्त सभी दर्शन, मनुष्य को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए, संग्रहित किए गए हैं जिनका, एकाग्रता से पालन किया जाना चाहिए| कभी आपने सोचा, क्यों जैन समाज व्यापार को प्राथमिकता देता है? यह जैन दर्शन का ही प्रभाव है जहाँ, कर्म प्रधान बताया गया और अपने भाग्य के लिए, अपने कर्मों को ही, आधार समझा गया जिससे, जैन दर्शन को मानने वाले लोगों में, क्रांतिकारी बदलाव हुए और आज कम जनसंख्या होने के बाद भी, मानव समाज में जैन व्यापारियों का प्रभाव देखा जाता है| उसी प्रकार यदि, पूर्ण बोध के साथ चार्वाक दर्शन का भी अनुगमन किया जाए तो, विषयासक्ति निष्क्रियता, मनुष्य को सत्य का आभास अवश्य कराएगी| जब मनुष्य अपने पूरी जागृति से, अपने सुखों की ओर देखता है तब, उसे आभास होता है कि, जो कभी उसका सुख था, वही आज उसका दुख बनने वाला है या बन चुका है और जब, यह दिखाई देने लगता है तो, चार्वाक मार्गी सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं क्योंकि, दैहिक सुखों को तो, लगभग सभी ने नकारने का प्रयत्न किया है अर्थात शारीरिक सुख को प्राथमिकता न देते हुए, अपने कर्मों पर केंद्रित होना ही, मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए किंतु, कर्म सत्य आधारित हो तभी, जीवन आनंददायी होगा| अब यहाँ, सत्य आधारित कर्म कैसे खोजे जा सकते हैं? तो, आपको बता दें कि, वह आपकी अंतरात्मा से ही प्रकट होंगे किंतु, जब व्यक्तिगत अहंकार मिट जाएगा और मन निजी स्वार्थ से हटकर, विचार करें तो, निश्चित ही मनुष्य अपना सत्य देख सकता है| हालाँकि, सत्य तो एक ही है, जिसके अनंत रूप है जो, सृष्टि के प्रारंभ से है और सदा रहेगा, न उसने जन्म लिया और न ही वह मरेगा| हाँ, मानव शरीर का अस्तित्व, अवश्य सीमित है जिसे, सत्य तक पहुँचने का साधन मात्र समझना चाहिए तभी, जीवन को सार्थक दिशा दी जा सकेगी|
